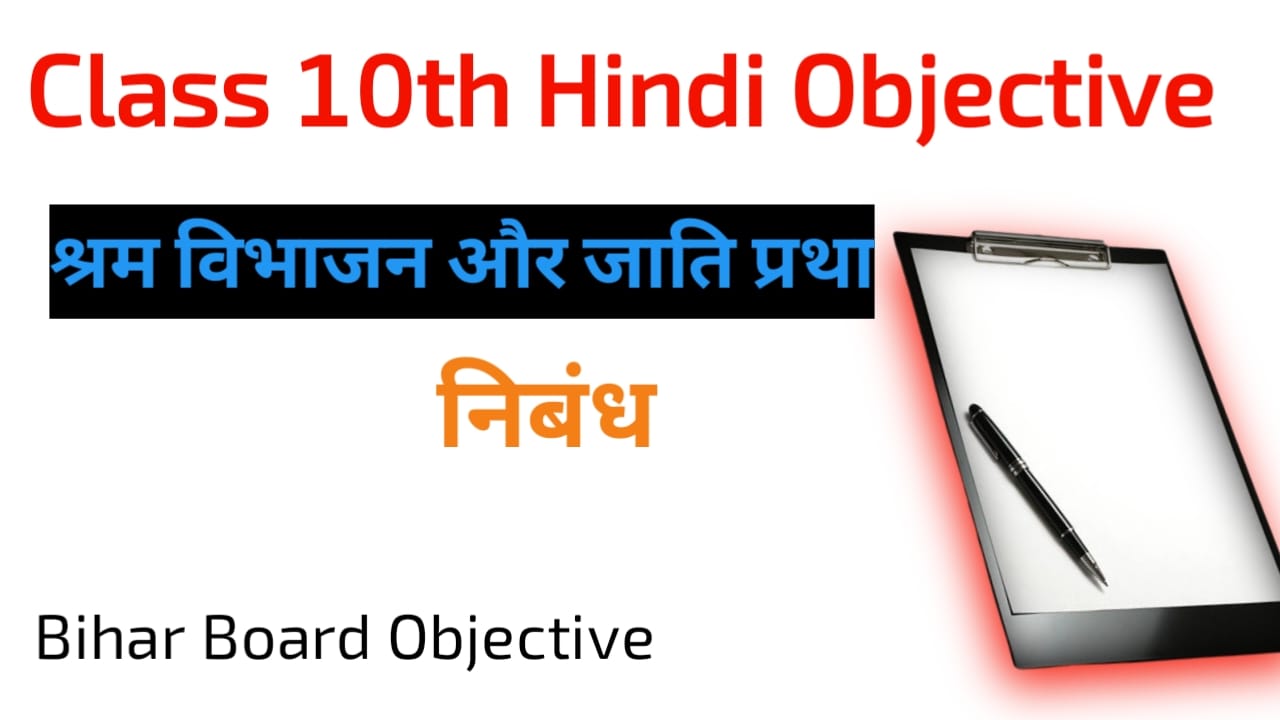×
श्रम विभाजन और जाति प्रथा भीमराव अंबेदकर
लेखक परिचय :
डॉ. भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 को मध्यप्रदेश के महू नामक नगर में एक दलित परिवार में हुआ था।
पिता का नाम – रामजी सकपाल
माता का नाम – भीमाबाई सकपाल
पत्नी का नाम – रमाबाई अंबेडकर
भीमराव अंबेदकर को मानव मुक्ति के पुरोधा भी कहा जाता है।
प्रारंभिक शिक्षा के पश्चात बड़ौदा नरेश के प्रोत्साहन से वे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए पहले न्यूयॉर्क (अमेरिका) गए और फिर लंदन (इंग्लैंड) भी गए। वर्ष 1916 में उन्होंने कोलंबिया विश्वविद्यालय से पीएच.डी. की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने समाज और राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए अछूतों, महिलाओं और श्रमिकों को उनके अधिकार व सम्मान दिलाने के लिए निरंतर संघर्ष किया।
बुद्ध, कबीर और ज्योतिबा फुले – ये तीन महान विचारक डॉ. भीमराव अंबेडकर के चिंतन और संघर्ष के मुख्य प्रेरणास्रोत थे।
प्रस्तुत पाठ डॉ. भीमराव आंबेडकर के प्रसिद्ध भाषण 'जाति का विनाश' ('एनिहिलेशन ऑफ कास्ट') से लिया गया है, जिसका हिंदी अनुवाद ललई सिंह यादव ने किया है। यह भाषण 'जाति-पाँति तोड़क मंडल' (लाहौर) के 1936 के वार्षिक सम्मेलन में अध्यक्षीय भाषण के रूप में लिखा गया था।
- बाबा साहेब ने अनेक पुस्तकें लिखी। उनकी प्रमुख एवं भाषण निम्नलिखित है
- (1). जेनेसिसि एंड डेवलपमेंट
- (5). बुद्धिज्म एंड कम्युनिज्म
- (6). बुद्धा एंड हिज धम्मा
- (7). थॉट्स ऑन लिंग्युस्टिक स्टेट्स
- (8). द राइज एंड फॉल ऑफ द हिंदू वीमेन
1. लेखक किस विडंबना की बात करते हैं? विडंबना का स्वरूप क्या है ?
उत्तर :- हमारे समाज में कुछ ऐसे भी लोग हैं जो जातिवाद का समर्थन करते. हैं। प्रकृति के अनुसार श्रम विभाजन आवश्यक है । परंतु यह आगे चलकर श्रमिक विभाजन का रूप धारण कर लेती है जिससे जाति प्रथा का जन्म होता है और समाज में ऊँच-नीच का भेदभाव पैदा हो जाता है। लेखक के लिए यही बात विडंबना है। बिडंबना का स्वरूप वर्ण-व्यवस्था है जिसके चार रूप हैं - ब्राह्ममण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ।
(2). जाति ,भारतीय समाज में श्रम विभाजन का स्वाभाविक रूप क्यों नहीं माना जा सकता है?
उत्तर :- जातिप्रथा मनुष्य की रुचि और कार्य क्षमता को नजरअंदाज कर उसे आजीवन एक ही पेशे में बाँध देती है वह चाह कर भी अपने पेशे को बदल नहीं सकता है।
3. भारत में जातिप्रथा किस प्रकार बेरोजगारी का एक मुख्य और स्पष्ट कारण बन गई है?
उत्तर :- आज के आधुनिक युग में उद्योग-धंधों का विकास, वैज्ञानिक आविष्कार और नई-नई तकनीकों की खोज निरंतर हो रही है, जिसके परिणामस्वरूप रोजगार के क्षेत्रों में अचानक परिवर्तन आ जाता है। लेकिन जाति प्रथा के बंधन के कारण व्यक्ति अपने पारंपरिक पेशे से हटकर नए अवसरों का लाभ नहीं उठा पाता। यही कारण है कि जाति प्रथा भूखमरी और बेरोजगारी को बढ़ावा देती है। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जाति प्रथा भारत में बेरोजगारी का एक प्रमुख और सीधा कारण बनी हुई है।
4. लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या किसे मानते हैं, और इसका क्या कारण बताते हैं?
उत्तर :- लेखक आज के उद्योगों में गरीबी और उत्पीड़न से भी बड़ी समस्या जाति प्रथा को मानते हैं क्योंकि श्रम विभाजन की दृष्टि से जाति प्रथा गंभीर दोषों से युक्त है। जाति प्रथा का श्रम विभाजन मनुष्य की इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। इसमें मनुष्य की रूचि और कार्य क्षमता का कोई स्थान नहीं है।
5. समाज में कुशल और सक्षम श्रमिकों के निर्माण के लिए किन बातों की आवश्यकता होती है?
उत्तर :- "समाज में कुशल और योग्य श्रमिकों का निर्माण तभी संभव है जब व्यक्तियों की रुचि को प्राथमिकता दी जाए। प्रत्येक व्यक्ति की क्षमता का ऐसा विकास होना चाहिए कि वह अपने पेशे या कार्य का चयन स्वतंत्र रूप से, अपनी इच्छा और योग्यता के अनुसार कर सके।"
6. लेखक के अनुसार, एक आदर्श समाज में कैसी गतिशीलता होनी चाहिए?
उत्तर: लेखक के अनुसार आदर्श समाज में ऐसी गतिशीलता होनी चाहिए कि कोई भी आवश्यक और सकारात्मक परिवर्तन समाज के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक आसानी से पहुँच सके।
7. जातिवाद के समर्थक उसके पक्ष में कौन-कौन से तर्क प्रस्तुत करते हैं?
उत्तर :- जातिवाद के पोषकों के अनुसार अगर कोई व्यक्ति आजीवन एक ही पेशा को अपनाए रहता है तो वह व्यक्ति उस पेशा में निपुण हो जाता है और अपना जीविकोपार्जन कर लेता है। अतः जातिवाद के पोषकों के अनुसार जाति प्रथा एक सही चीज है।
8. लेखक ने जातिवाद के समर्थन में दिए गए तर्कों पर क्या मुख्य आपत्तियाँ व्यक्त की हैं?
उत्तर :- जातिवाद के पक्ष में दिए गए तर्कों पर लेखक का कहना है कि जातिप्रथा श्रम विभाजन के साथ-साथ श्रमिकों का भी विभाजन कर देती है। उसे वह आजीवन एक ही पेशे में वाँध देती है। वह अपनी रूचि के अनुसार किसी भी कार्य का चुनाव नहीं कर पाता है। अतः यह विभाजन अनुचित है।
9. लेखक ने पाठ में जातिप्रथा को किन प्रमुख कारणों से हानिकारक बताया है?
उत्तर :- "जातिप्रथा के चलते अनेक लोग ऐसे कार्य करने को मजबूर होते हैं, जिनमें उनकी कोई रुचि नहीं होती। वे केवल सामाजिक दबाव और विवशता के कारण उस कार्य को अपनाते हैं। जब कोई व्यक्ति बिना मन और रुचि के कार्य करता है, तो न उसमें लगन होती है और न ही दक्षता विकसित हो पाती है। परिणामस्वरूप कार्य की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसलिए आर्थिक दृष्टि से जातिप्रथा एक अत्यंत हानिकारक व्यवस्था है।"
10. सच्चे लोकतंत्र की स्थापना के लिए लेखक ने किन विशेषताओं को ज़रूरी माना है?
उत्तर :- सच्चे लोकतंत्र के लिए समाज में स्वतंत्रता,समानता एवं भाईचारे का भाव होना आवश्यक है। इसमें यह आवश्यक है कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा एवं सम्मान का भाव हो।